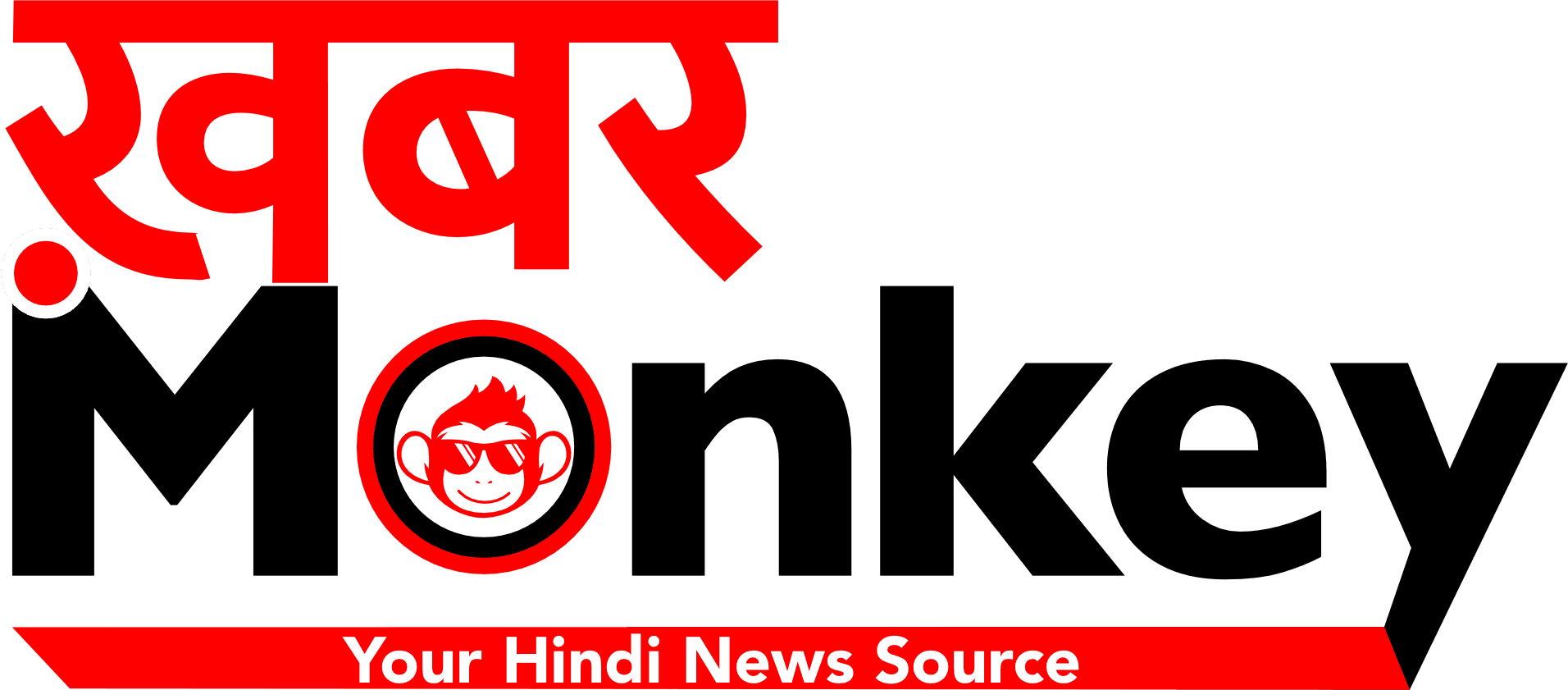‘द कश्मीर फाइल्स’ और इसी सीरीज़ पर पिछले कुछ सालों में आई फिल्मों पर बात करने से पहले मैं विषय प्रवर्तन के लिए अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे बॉलीवुड में लोकप्रिय पिता के दिवंगत होने के बाद उनकी कमतर प्रतिभा वाली संतान द्वारा पूरे आत्मविश्वास और अधिकार के साथ आधी सच्ची आधी झूठी बात कहने की परंपरा रही है। इन दिनों एक किस्सा गीतकार आनंद बक्षी के बेटे राकेश आनंद बक्षी विभिन्न मंचों पर लगातार दोहरा रहे हैं कि उनके दिवंगत पिता आनंद बक्षी को अपनी इस गलती पर बरसों पछतावा होता रहा कि ‘अंधा कानून’ फिल्म के मुस्लिम चरित्र जां निसार अख्तर (अमिताभ बच्चन) के लिए कैसे उन्होंने ‘जितनी चाभी भरी राम ने उतना चले खिलौना’ लिख दिया। यदि उन्हें ज़रा भी इल्म होता कि वह मुस्लिम चरित्र है, तो वे ऐसा गीत कतई नहीं लिखते।
एक आम गीत-संगीतप्रेमी होने के नाते हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि राकेश आनंद बक्षी का यह कथन भ्रामक हो। लेकिन यदि यह सही है तो उन्हें कौन समझाए कि ‘जितनी चाभी भरी राम ने, उतना चले खिलौना’ हमारे लोक में एक कहावत के रूप में प्रयुक्त की जाती है और इसका किसी धर्म-जाति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि बाप-बेटे इस पंक्ति को धर्म विशेष से जोड़ना ही चाहते हैं तो उन्हें इस बात का भी अफसोस करना चाहिए कि उन्होंने ‘दोस्ताना’ फिल्म के हिंदू नायक विजय (अमिताभ बच्चन) द्वारा अपने हिंदू दोस्त रवि (शत्रुध्न सिन्हा) के लिए ‘मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है के तू बेवफा हो गया’ के अंतरे में ‘खुदा जाने क्या माजरा हो गया’ लिखने जैसी भूल क्यों कर दी? यही बक्षी साहब ‘आन मिलो सजना’ में हिंदू पात्र अजीत (राजेश खन्ना) और वर्षा (आशा पारेख) के बीच ‘अच्छा तो हम चलते हैं’ गीत में ‘जुम्मे रात को’ लिखने के बाद पछताए या नहीं? यदि हमारी फिल्म इंडस्ट्री धर्म के मामले में इतनी ही संवेदनशील है तो न तो हसरत जयपुरी ‘हरियाली और रास्ता’ में हिंदू पात्र के लिए ‘इब्तिदा-ए-इश्क़ में हम सारी रात जागे अल्ला जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे’ लिखते और न ही मजरूह सुल्तानपुरी साहब ‘मेरे हमदम मेरे दोस्त’ में मीना (मुमताज़) से ‘अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में’ गवाते।
सच तो यह है कि हिंदू समाज बहुत उदार और सहिष्णु रहा है। बरसों वह इसी उदार दृष्टिकोण से चला कि समाज में समता, समरसता हो, सब धर्मों का सम्मान हो। लेकिन बॉलीवुड ने इस उदार दृष्टिकोण का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, कभी अनजाने में तो कभी एक खास एजेंडे को चलाने के लिए। जब तक सिनेमा में सहजता की धारा बहती रही, तब तक दर्शक भी उसे सहजता से स्वीकार करते रहे। लेकिन नब्बे के दशक में सिनेमा में अन्डरवर्ल्ड की दखल बढ़ जाने के बाद एक खास प्लानिंग के जरिए खान त्रयी को आगे बढ़ाया गया, पाकिस्तान से गायकों-संगीतकारों की फौज बुलवाई गई और नब्बे प्रतिशत गीतों में मधुरता की उपेक्षा करते हुए ‘अल्लाह’, ‘मौला’, ‘खुदा’ टाइप के शब्द बिना संदर्भ के ठूँसते हुए सिने-संगीत को रसातल में पहुंचाने की चेष्टा की गई।
विज्ञान का नियम है, हर क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज जो हम ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘द केरला स्टोरी’ और ‘द बंगाल फाइल्स’ जैसी फिल्मों का चलन देख रहे हैं, वह बॉलीवुड द्वारा पैंतीस साल शराफत से और फिर पैंतीस साल ढीठता से चलाए गए एजेंडे की ही प्रतिक्रिया मात्र है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरला स्टोरी’ की सफलता तो अभूतपूर्व है। जहां ‘द कश्मीर फाइल्स’ में 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर किए अत्याचार और फलस्वरूप उनके पलायन का चित्रण है, वहीं ‘द केरला स्टोरी’ में केरल में ‘लव जेहाद’ के तहत हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करवाकर उनसे शादी करने और फिर उन पर अत्याचार और जुल्म ढाने की सच्ची, दुखद और कड़वी सच्चाई को रेखांकित किया गया है। इसी श्रेणी की नवीनतम फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ अविभाजित बंगाल में चालीस के दशक में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर है।
बरसों पंडे-पुजारियों को धूर्त, पाखंडी और लंपट दिखाने वाले सिनेमा का कायांतरण होकर मुल्ला-मौलवियों को दुष्ट दिखाने का यह अंदाज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इन फिल्मों का खूब विरोध किया। विरोध करनेवालों की इस टोली में मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले कई राजनीतिक दल, पिछले एक दशक से सत्ता की मलाई से प्रवंचित पत्रकार-लेखक और विश्वविद्यालयों में ‘लेके रहेंगे आजादी’ टाइप के नारे लगाने वाले विद्यार्थी और प्रोफेसर शामिल थे। यह समाज का वही खाया पिया अघाया वर्ग है, जिसे ‘गदर’ में सनी देवल द्वारा पाकिस्तान जाकर हैन्ड पम्प उखाड़ने से भी नाराज़गी है और थियेटरों में ‘जन गण मन’ गाने में असुविधा भी। देश के किसी भी गाँव-कूचे में किसी खास मजहब के एक भी व्यक्ति पर हुए अत्याचार पर सारे देश में मोमबत्तियाँ जलाने वाले और शेष बचे नागरिकों में से किसी के साथ भी हुई घनघोर से घनघोर ज्यादती पर शरारती चुप्पी ओढ़ लेने वाले इस वर्ग की बेचैनी स्वाभाविक है।
सवाल यह है कि यकायक सिनेमा में ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों का उदय कैसे हो गया? वस्तुतः सिनेमा को कई कलाओं का संगम माना गया है। इन कलाओं में कहानी, संवाद, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, एक्शन, नाटकीयता, भावनात्मकता जैसे बहुविध मानवीय और कलात्मक पक्ष शामिल हैं। बरसों सिनेमा इन्हीं कलाओं पर केंद्रित रहा, लेकिन कोरोनाकाल के दौरान मध्यवर्ग के बीच आए ओटीटी के उभार ने सिनेमा और धारावाहिकों में कथ्य की प्रधानता को रेखांकित किया। यही कारण था कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद जहां ‘दृश्यम-2’, ‘भूल भुलैया-2’ और ‘स्त्री-2’ जैसी कथानक के आधार पर पूर्व में स्वीकृत फिल्मों के सीक्वल को सफलता मिली, वहीं ‘लापता लेडीज़’ व ‘12 वीं फैल’ जैसी उद्देश्यपूर्ण फिल्मों को भी आम दर्शकों द्वारा सराहा गया। सिनेमा में आए इस यू-टर्न ने विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्त सेन जैसे फ़िल्मकारों को सिनेमा के फॉर्मेट में बिना डरे, बिना झिझके सत्य को दिखाने के लिए प्रेरित किया। इसी के चलते दर्शकों को ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘द केरला स्टोरी’ और ‘द बंगाल फाइल्स’ जैसी देखने को मिलीं। इन तीनों फिल्मों में तत्कालीन समय की हिंसा, क्रूरता, पाशविकता को इतने सूक्ष्म तरीके से चित्रित किया गया कि अतीत में मिले जख्म फिर से हरे हो गए और दर्शक फिल्म देखने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए आंसुओं में भीगे हुए, उदास, खिन्न और गुस्से में दिखलाई दिए।
निश्चित ही यह वह सिनेमा नहीं था, जिसे दर्शक बरसों तक देखते रहे हैं। यह भी सही है कि ये फिल्में न तो सिनेमा को कला मानने की अवधारणा पर खरी साबित हुईं और न ही जिस बॉलीवुड की देश-दुनिया में पहचान है, उसे स्थापित कर पाने में सफल हो सकीं। यह भी सच है कि इसी पैटर्न पर आने वाले समय में कुछ और फिल्में बन सकती हैं, लेकिन उन फिल्मों की सफलता संदिग्ध ही है। पिछले दिनों प्रदर्शित ‘द बंगाल फाइल्स’ की असफलता यह दर्शाती है कि जिन दर्शकों ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों को पसंद किया है, वे भी न तो ऐसा समाज चाहते हैं, जिसका इन फिल्मों में उल्लेख किया गया है और न ही ऐसी फिल्मों की निरंतरता बनाए रखने को प्रेरित करने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति। अहिंसा, समता, समरसता के सिद्धांत पर चलता आया हमारा समाज आज सिनेमा में भी एक बेहतर समाज की ही चाहना रखता है। अब यह हमारे नीति-नियंताओं पर निर्भर करता है कि वे कैसा समाज बनाते हैं और फलतः कैसी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।