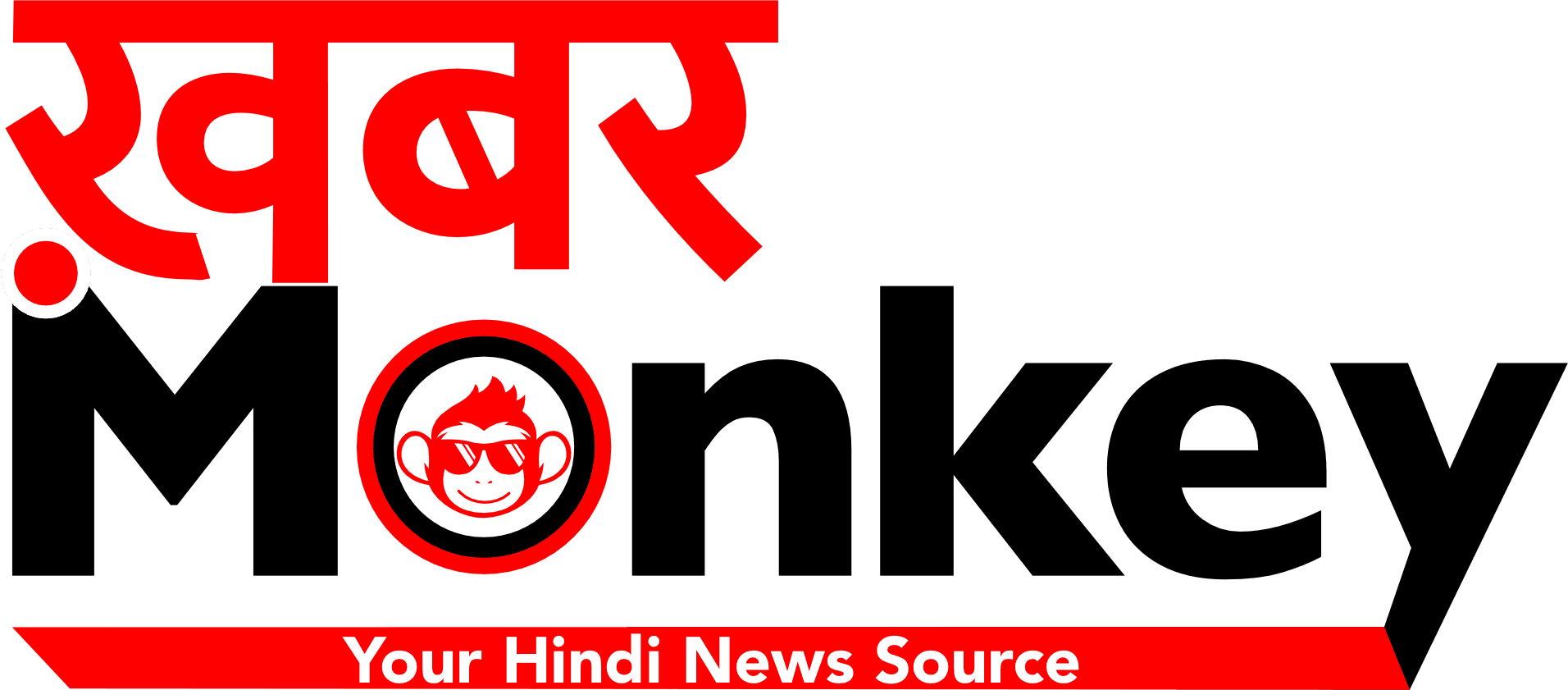कुष्ठ रोग पर काबू
कुष्ठ रोग, जिसे हन्सेन के नाम से भी जाना जाता है. ये रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है. इसके संक्रमण की वजह से शरीर पर कई तरह के धब्बे पड़ जाते हैं. संक्रमित एरिया को अगर छुआ जाए तो वो लगभग सुन्न सा रहता है. वहां पर दर्द, गर्मी या फिर ठंड किसी चीज का भी अहसास नहीं होता है. जो इस बीमारी से ग्रसित है उसके शरीर के कई हिस्सों जैसे पैर, हाथ या चेहरे में बदलाव देखे जा सकते हैं यानी टेढ़ापन भी इस बीमारी का अहम लक्षण है. साथ ही आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. आंखों से कम दिखना, बंद करने में दिक्कत जैसी समस्याएं शामिल हैं.
संक्रमण पर कैसे हुआ रोकथाम?
1951 की जनगणना के मुताबिक, कुष्ठ रोग एक आम समस्या थी. यहां कुल आबाद में से 13,74,000 लोग ऐसे थे कुष्ठ रोग से संक्रमित थे. यानी हर 10 हजार लोगों पर 38 लोग कुष्ठ रोग से संक्रमित थे. ऐसे में सरकार की तरफ से इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी गई और इसकी रोकथाम के लिए काम शुरू किया गया. सबसे पहले तो 1954-55 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (NLCP) चलाया गया. इस योजना के तहत घर-घर जाकर डैप्सोन मोनोथेरेपी के अंतर्गत संक्रमित शख्स का इलाज शुरू किया गया. इस संक्रमण पर और काबू पाने के लिए 1969-74 में कार्यक्रम को और ज्यादा स्तर पर बढ़ाया गया. चौथी पंचवर्षीय योजना में इस संक्रमण पर शहर और गांव स्तर पर इसके कवरेज को बढ़ाया गया.
NGOs की भागीदारी बढ़ाई
कुष्ठ रोग पर काबू पाने के लिए 1983 में NGOs की भागीदारी बढ़ाई गई. इसके तहत SET यानी सर्वे, शिक्षा, उपचार की योजना शुरू की गई, जिसमें NGOs की मदद से कुष्ठ रोगियों की पहचान और उनके इलाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया. यहां हर 25 हजार की आबादी पर पैरामेडिकल कर्मचारी को नियुक्त किया गया. इसके बाद अब लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरुकता फैलाई गई.
घर-घर जाकर सर्वे की मदद से लोगों को इसके संक्रमण के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया गया ताकि संक्रमण के शुरुआती दिनों में इसका इलाज करा सकें. लोगों को क्लीनिक जानकारी में शामिल किया गया. 1982-83 में MDT की शुरुआत हुई, जिसमें मल्टी ड्रग थेरेपी को शुरू किया गया. इसे WHO की तरफ से मान्यता दी गई थी. इसे देश में इस बीमारी को कम करने और हराने के लिए इसका फ्री इलाज और सलाह भी शुरू किया गया.
संक्रमण के आंकड़ों में आई गिरावट
1981 में कुष्ठ रोग की दर 57.2 प्रति 10,000 थी, जो मार्च 1984 तक 44.8 और मार्च 2004 तक 2.4 प्रति 10,000 हो गई. 1981 में नए मरीजों में गंभीर विकृति (ग्रेड II) की दर 20% थी, जो 2004 तक 1.5% रह गई. विश्व बैंक ने 1993-2000 और 2001-2004 के दो प्रोजेक्ट्स के जरिए सामुदायिक भागीदारी और IEC नई तकनीकों की मदद ली गई. NGOs, WHO, Danida, और BBC WST, SOMAC, Lintas जैसे मीडिया संगठनों के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ाया गया. 2004 तक, 17 राज्य और 250 जिले कुष्ठ रोग उन्मूलन (प्रति 10,000 पर एक से कम मामले) के लक्ष्य को हासिल कर चुके थे, और 7 राज्य इसके करीब थे. दिसंबर 2005 तक भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग को हराने का लक्ष्य हासिल कर लिया.
आगे की राह
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के तहत 2023-2027 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और रोडमैप तैयार किया गया, जो 2030 तक कुष्ठ रोग के प्रसार को पूरी तरह रोकने और विदेशी मामलों के संक्रमण न फैल सके.वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति 2021-2030 के तहत इसके साथ ही मजबूत निगरानी, डिजिटलीकरण, वैक्सीन की शुरुआत और जागरूकता अभियानों पर जोर दिया गया. जिला स्तर पर पांच साल तक बच्चों में कोई नया मामला न आए और फिर तीन साल तक कोई नया मामला न हो. इस पर काम किया जा रहा है.