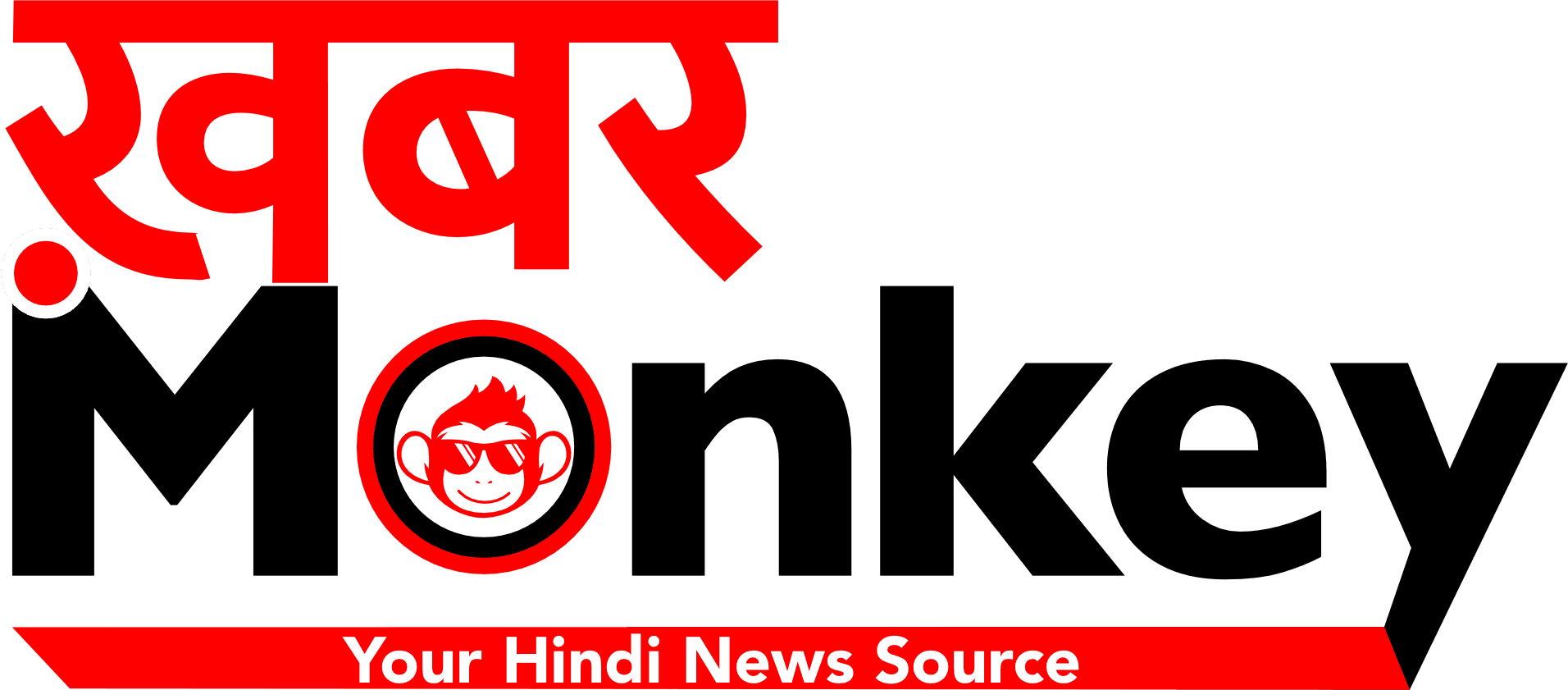2025 की विजय दशमी वार्षिक पर्व नहीं, वरन् एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के एक सौ वर्ष पूरे हुए। संघ का लक्ष्य किसी एक दो या अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं वरन् हिन्दू-राष्ट्र से शक्ति प्राप्त करना और फिर उसे और शक्तिशाली बनाना है। राजनैतिक मंच जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) के दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने दर्शन “एकात्म मानवतावाद” के माध्यम से सामाजिक स्तर “सामाजिक समरसता” को केन्द्र में रखा। समरसता के आदर्श भगवान श्री राम हैं जिन्हें इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग को “समरस” किया और कभी भी स्थापित सामाजिक मूल्यों और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। सामाजिक परंपराओं और स्थापित मूल्यों के अंतर्गत रहकर उन्होंने सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना की। उन्हें समरसता का नायक भी कहा जाता है। लेकिन क्यों और कैसे? इसी के आलोक में विजय दशमी पर “समरसता के नायक राम” पर मेरे विचार।
इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है की समरसता क्या है? यदि हम इसकी शाब्दिक व्याख्या करें तो यह दो शब्दों से बना है- सम और रस। साहित्य और व्याकरण में रस उस “अनुभूति” को कहा जाता है जो किसी साहित्य को पढ़ने के बाद मन में उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में वह “भाव” जो अनुभूत होता है – रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है – आनन्द। काव्य में जो आनन्द आता है, वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनन्द अर्थात् रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है कि “रसात्मकम् वाक्यम् काव्यम्” अर्थात् रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। विस्तारित अर्थों में यदि कहें तो किसी के कार्य या आचरण को देखकर, कोई नाटक या दृश्य देखकर, कोई वाणी या विचार सुनकर, मन में जो “भाव” पैदा होता है। उसे हम रस कहते हैं। संतो के द्वारा ईश्वर का गुणगान करने और उसकी व्याख्या सुनकर मन में भक्ति का भाव पैदा होता है जो भक्ति रस है। वीर पुरुषों की गाथा सुनकर या उनके वीरोचित कर्म देखकर, या उनकी वीरता को जानने पर मन में वीर रस की अनूभूति होती है। किसी प्रेयशी के सौंदर्य वर्णन या सौंदर्य को देखकर श्रृंगार रस की अनुभूति है। जब हम किसी को अपराध करते हुए, अत्याचार करते हुए देखते हैं या ऐसे विषयों को पढ़ते तो मन में पैदा होने वाली अनुभूति घृणा रस या रौद्र रस है।
एक प्रसिद्ध सूक्त है- रसौ वै स:। अर्थात् वह परमात्मा ही रस रूप आनन्द है। “कुमारसम्भव” में जल, तरल और द्रव के अर्थ और प्रेम की अनुभूति के लिए रस शब्द का प्रयोग हुआ है। “रघुवंश” में आनन्द और प्रसन्नता के अर्थ में रस शब्द काम में लेता है। आयुर्वेद में रस छह माने गए हैं- कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। वैशेषिक दर्शन में चौबीस गुणों में एक गुण का नाम रस है।
उपरोक्त शब्द प्रमाण से यह स्पष्ट है की रस वह मनोभाव या अनुभूति है जो किसी साहित्य के अध्ययन या किसी पुरुष के क्रियाकलापों को, कार्यों को, जीवन चरित्र को देखकर मन में उत्पन्न होता है। चूंकी विषय “समरसता” का है तो “सम” को भी समझना आवश्यक है। सम का तात्पर्य सामान्यतः “समान” या “ समतुल्य” से लिया जाता है। तो समरसता यानी “एकरस” होना। जिस प्रकार दूध, जल, शक्कर, मधु, दही मक्खन इत्यादि को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जो रस पैदा होता है वह इन सभी द्रव्यों के रस का एकरस है न की “समुच्चय”। यह इनमें से किसी का रस नहीं होता बल्कि इन सब के सम्मिश्रण का एक नवरस पैदा होता है। इस प्रकार जब हम समरस की बात करते हैं तो तात्पर्य यह होता है कि हम अनेक रसों से “एकरस” हों। जब हम समरसता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि अनेक रस मिलाकर जब एकरस हो जाए।
आज के परिवेश में “सामाजिक समरसता” पर काफी विचार और बहस होती है। सामाजिक समरसता का तात्पर्य न तो सभी का समान हो जाना है न ही अपने अस्तित्व को खोना है। वरन् उन उच्च मूल्यों को धारण कर एकरस होना है। अनेक विदूषक सामाजिक समरसता के नाम पर यह दिखाने का प्रयास करते हैं की हमें भी उन्हीं मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए जो समाज में स्वीकार्य नहीं रहे हैं। ऐसा कर हम सामाजिक समरसता स्थापित कर लेंगे। परन्तु यह अभिधारणा ही अनुचित है। सामाजिक समरसता एकरस होना है किन्तु हमारी गति उर्ध्वगामी होने चाहिए, अधोगामी नहीं। यह पिछड़े, दब, कुचले को अपने सम लाना है न की उनके सम हो जाना है। यही प्रगति है और यही हमारे आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण ने किया।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम चूंकी ईश्वर के साक्षात अवतार है तो वह स्वयं सभी रसों का श्रोत है। सभी रस वहीं से निकलते और वही एकरस हो जाते हैं। वह सबको अपने रस में ढाल लेते हैं। शबरी के जूंठे बेर खाकर उन्होंने जो समरस पैदा किया वह उनका रस था या शबरी का? क्योंकि सभी रस पहले से ही भगवान श्री राम में समाहित है इसलिए जो भी उनसे मिलता है उन जैसा ही हो जाता है। यदि हम सामाजिक धरातल पर देखते हैं तो भगवान श्रीराम सामाजिक समरसता के अप्रतिम उदाहरण हैं। राम वन गमन के समय पहली रात वह निषाद के नगर में उनके सानिध्य में बिताते हैं। नदी के उस पार ले जाने का अनुरोध करते हैं। उनका जो समता और भ्रातृत्व का व्यवहार गुह्यराज (निषादराज) के साथ होता है उससे निषादराज अत्यन्त भाव विह्वल हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं श्रीराम उनका आथित्य स्वीकार कर उनके घर पधारें। श्रीराम यह कहकर अनुरोध को अस्वीकार करते हैं की वह वनवासी हैं और उन्हें नगर में जाने की अनुमति, पिता की आज्ञानुसार, नहीं है। किन्तु वह अपने सखा और सहपाठी निषादराज को यह आश्वासन देते हैं की 14 वर्षों का वनवास पूरा कर लौटते समय वह निषाद राज का आतिथ्य अवश्य स्वीकार करेंगे। अपने सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के प्रति उनका व्यवहार भातृवत है। उसमें राजा-प्रजा, ईश्वर -आत्मा, बृहद-लघु उच्च-नीच का कोई भेदभाव नहीं है। प्रेम एक रस है और वह प्रेम रस के भूखे हैं। इसी तरह शबरी के साथ उनका समरस हो जाना अपने आप में एक अप्रतिम उदाहरण है। भीलनी के जूंठे फल वह इतनी आत्मीयता से खाते हैं जैसे उन्हें यह पता ही नहीं हो कि यह पहले से जूंठे कर दिए गए हैं। लक्ष्मण के बार-बार संकेत करने पर भी वह उसे अनदेखा कर देते हैं और मीठे फलों की प्रशंसा में इतने अभीभूत हो जाते हैं की भीलनी तो कभी समझ ही नहीं पाती कि उसने ऐसा कुछ किया है जो सामाजिक स्तर पर स्वीकार्य नहीं होता। भाव के धरातल पर शबरी और भगवान श्रीराम एक रूप है। दोनों के बीच प्रेम की जो धारा बहती है उसमें दोनों का अस्तित्व अलग-अलग नहीं है।
इसी प्रकार लंका विजय के पहले वानर और भालुओं की सेना में एक-एक भालू और बंदर अपने को राम मय समझता है। एकरसता ऐसी कई सभी को लगता है वह उसका व्यक्तिगत अभीप्सित है। वे अपने को एकोद्देश्य कर लेते हैं और भावनात्मक रूप से भगवान श्री राम से एकीकृत हो जाते हैं। श्रीराम की यही शक्ति है। उनके निकट आने वाला अपने को उनसे अलग नहीं समझता। इतना ही नहीं परम शत्रु रावण का अनुज विभीषण जब उनके शरण में आता है तो श्रीराम उसका उठकर स्वागत-सम्मान करते हैं और अपने निकट बिठाते हैं। जो भी उनके निकट आता है वह अपने को समरूप और एक रूप पाता है। यह स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है की समरस का तात्पर्य सभी की समानता नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है की श्रीराम निषाद राज या शबरी के रस में बदल गये वरन् यह है कि उन्होंने अपने रस में अपने में सभी को समाहित कर लिया। ईश्वर मानवीय नहीं होता मानव ईश्वर मय होता है। यही जीवन का परम लक्ष्य भी है। यह प्रकृति का नियम है की गति निम्न से उच्च, अपूर्ण से पूर्ण और आत्म से परमात्म की ओर होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह या तो अगति (जड़ता) है या दुर्गति (पतन) है, प्रगति नहीं है।
ज्ञान, भक्ति और योग यह ईश्वर के प्राप्ति के जो तीन मार्ग हैं उनमें भी परम उद्देश्य ईश्वर मय हो जाना है, राममय हो जाना है। ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा ईश्वर को समझना और इस बात की अनुभूति कर लेना कि मैं वही हूं- “तत्वमसि” और “अहम् ब्रह्मास्मि”। यह शोधक और शोध्य का एकरस होना है। भक्ति मार्ग में भी समरस का यही अर्थ बताया गया है। जैसे कबीर कहते हैं:
लाली मेरे लाल की
जित देखो तित लाल
लाली देखन मैं गई
मैं भी हो गई लाल।
इसमें संपूर्ण समर्पण भाव है जहां भक्त अपने रस को उस परम रस में सम्मिलित करने की ही बात करता है। कपिन्याय हो या मार्जारन्याय हो, स्वरूप एकरूप और एकरस होना ही है। योग मार्ग में तो स्पष्ट यही बात कही गई है। “समत्वं योगमुच्यते” यानी “समत्व” ही योग है। जब हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं तो वही योग है। जिसका तात्पर्य होता है जुड़ जाना और अनेकरस से एकरस और समरस हो जाना।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम अलौकिक विश्व में भगवान विष्णु के अवतार थे किन्तु लौकिक विश्व में एक युग पुरुष भी थे। उनका अवतार और जन्म ही सनातन मूल्य की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। सत्य सनातन संस्कृति का यह स्थापित मूल्य है, कि जब-जब धर्म का ह्रास होता है, असुर, दानव और अत्याचारी अनाचारी बढ़ने लगते हैं, नकारात्मक और अनिश्वरवादी शक्तियां प्रबल होने लगते हैं, समाज में सनातन मूल्यों का ह्रास होने लगता है तो इन सनातन मूल्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इसका प्रमाण हमारे लगभग सभी महान ग्रंथों मे है। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते हैं-
जब जब होइ धर्म की हानि
बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी।
तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा
हरहीं कृपा निधि सज्जन पीरा।
इसी बात को कई हजार वर्ष बाद श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए समझाते हैं-
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत:। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥
“हे अर्जुन! जब धर्म का ह्रास होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने को अवतरित करता हूं। सज्जनों के परित्राण के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मै युगों युगों में जन्म लेता हूं।”
सही अर्थों में समरसता की स्थापना ईश्वरावतार का एक प्रमुख उद्देश्य है।